भाव पल्लवन किसे कहते हैं | भाव विस्तारण का उदाहरण क्या है , परिभाषा , वाक्य bhav pallavan in hindi
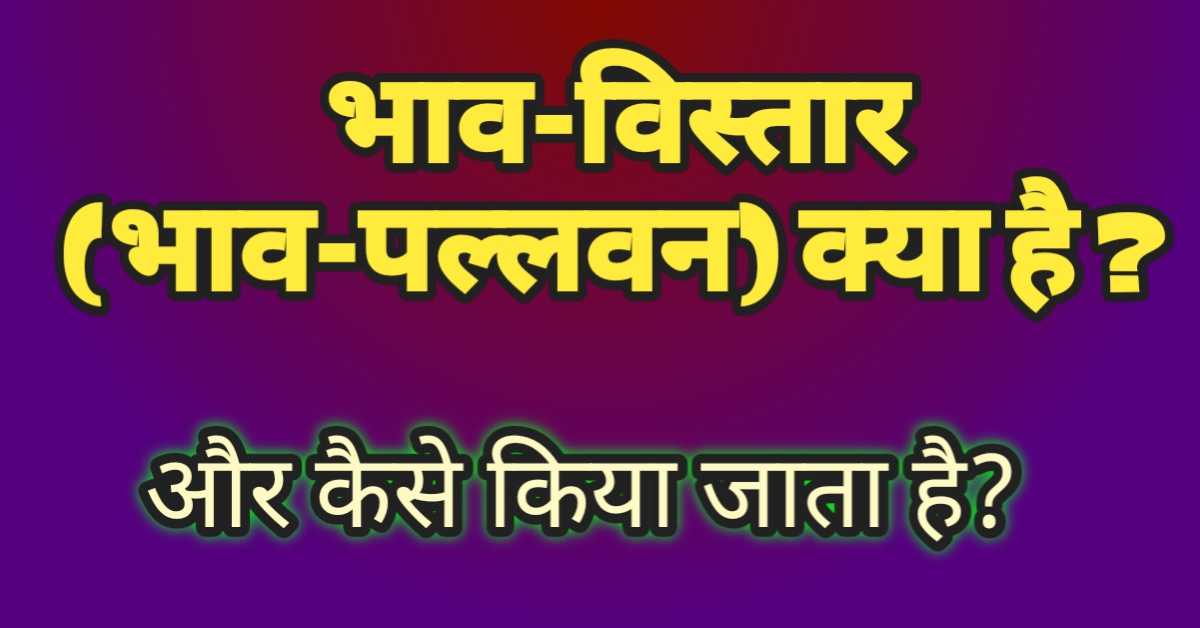
bhav pallavan in hindi kaise kare पल्लवन का उदाहरण दीजिए , भाव पल्लवन किसे कहते हैं | भाव विस्तारण का उदाहरण क्या है , परिभाषा , वाक्य कैसे करें ?
भाव- पल्लवन या भाव – विस्तारण
जब किसी सुगठित और गुंफित विचार अथवा भाव को विस्तार दे दिया जाता है, उसे भाव-पल्लवन या भाव-विस्तारण कहते हैं । सघन रूप में कम से कम शब्दों के माध्यम से जब लेखक अपने विचारों को प्रस्तुत करता है, वैसी स्थिति में सामान्य पाठक आसानी से इन विचारों को ग्रहण नहीं कर सकता। जो वाक्य ‘गागर में सागर‘ की तरह होते हैं वे साधारण लोगों की समझ में नहीं आते । ऐसे वाक्यों में सन्निहित विचारों या भावों के तार-तार को अलग कर उनकी व्याख्या करनी पड़ती हैय उनकी गुत्थी को सुलझाना पड़ता है। भावविस्तार या भावपल्लवन में मूलवाक्य में आये विचार सूत्रों को सही अर्थ में समझने की चेष्टा की जाती है और उन्हें विस्तार से समझाया जाता है।
भावपल्लवन भावसंक्षेपण का ठीक उलटा होता है । भावपल्लवन भावार्थ व्याख्या से भिन्न होता है । व्याख्या और भावपल्लवन दोनों में मूल अवतरण के भाव अथवा विचार को विस्तार दिया जाता है । लेकिन व्याख्या में प्रसंगनिर्देश अनिवार्य होता है, साथ ही इसमें विचारों की आलोचना एवं टीका-टिप्पणी भी की जाती है । यह छूट भावपल्लवन में नहीं है । भावपल्लवन में केवल निहित भाव अथवा विचार का विस्तार होता है । भावार्थ और भावपल्लवन दोनों में मूलभाव को स्पष्ट किया जाता है, लेकिन भावार्थ में मूल भाव का विस्तार एक सीमा तक ही होता है, जबकि भावपल्लवन के लिए ऐसी किसी सीमा का बन्धन नहीं है । भावपल्लवन में यह प्रयत्न किया जाता है कि मूल लेखक के मनोभाव व्यक्त हो जायँ अर्थात् समस्त मनोभाव को व्यक्त करने के लिए कई अनुच्छेदों में लिखा जाता है । भावार्थ में तो मूल अवतरण के केन्द्रीय भाव को ग्रहण किया जाता है, जिसे कई अनुच्छेदों में लिखना आवश्यक नहीं है । भावपल्लवन में तो केन्द्रीय भाव के साथ गौण भाव को भी ग्रहण कर विस्तार से उनका विश्लेषण किया जाता है। इस प्रकार भावपल्लवन व्याख्या और भावार्थ से भिन्न है।
भावपल्लवन अथवा भावविस्तारण के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना जरूरी है-
1. भावपल्लवन के लिए मूल अवतरण के रूप में कोई प्रसिद्ध वाक्य, सूक्ति, लोकोक्ति अथवा कहावत दे दी जाती है । वस्तुतः इन्हें बार-बार पढ़ना चाहिए जिससे पूरा का पूरा भाव या विचार समझ में आ जाय ।
2. मूल भाव या विचार के साथ चिपके हुए अन्य सहायक भावों को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए।
3. सभी मूल एवं गौण भावों या विचारों को समझ लेने के पश्चात् उनका क्रम निर्धारित कर लेना चाहिये। इसके बाद प्रत्येक विचार को अलग-अलग एक-एक अनुच्छेद में लिखना
4. विचारों का विस्तार करते समय उनकी पुष्टि के लिए यत्र-तत्र ऊपर से कुछ तथ्य अथवा उदाहरण दिये जा सकते हैं।
5. भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। अलं-त भाषा नहीं लिखनी चाहिए । छोटे-छोटे वाक्यों के माध्यम से भावों, विचारों को व्यक्त करना चाहिए ।
6. भावपल्लवन में अनावश्यक बातों का उल्लेख नहीं होना चाहिए ।
7. इसमें मूल लेखक के भावों, विचारों का ही विस्तार एवं विश्लेषण करना चाहिए, उनकी टीका-टिप्पणी अथवा आलोचना नहीं करनी चाहिए ।
8. भावपल्लवन अन्य पुरुष में लिखना चाहिए ।
9. इसमें समास शैली को न ग्रहण कर व्यास शैली ग्रहण की जाती है।
10. यदि हम उक्ति या मूल लेखक के कथन से सहमत नहीं हैं तो भी उसका खंडन हम नहीं कर सकते। भावपल्लवन में तो उक्ति अथवा कथन को विस्तार के साथ स्पष्ट किया जाता है।
उदाहरण के लिए एक भावपल्लवन नीचे दिया जा रहा है-
सागर के समान कामना-नदियों को पचाते हुए सीमा से बाहर न जाना यही तो ब्राह्मण का आदर्श है।
भावपल्लवन–
पावस ऋतु में नदियाँ उन्मत्त होकर छलछलाती हुई प्रवाहित होती हैं और ग्रीष्म के आने पर शांत हो जाती हैं । परन्तु समुद्र का जल-तल प्रत्येक ऋतु एवं समय में एक समान रहता है । इसीलिए उसे ‘सम़उद्र‘ ‘सदैव समान जलवाला‘ कहा गया है। पावस ऋतु में न तो उसमें जलप्लादन ही आता है और न तो ग्रीष्म ऋतु में जल कम होता है । यदि अनेकानेक उमड़ती हुई वेगवती नदियाँ भी एक समुद्र में प्रवेश करें, तो भी उसके गांभीर्य में कोई हास नहीं होता । सच्चे ब्राह्मण का व्यक्तित्व भी समुद्रवत् होता है । बड़े-बड़े प्रलोभन के आने पर भी ब्राह्मण अपनी मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करता। श्री जयशंकर ‘प्रसाद‘ द्वारा लिखित ‘चन्द्रगुप्त‘ नाटक के चाणक्य नामक पात्र के व्यक्तित्व में यह आदर्श द्रष्टव्य है । चाणक्य अपनी कामनाओं को अपने वश में रखते हुए सम्राट् चन्द्रगुप्त का सहायक होता है । अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए बाल्यकाल की प्रिया सुवासिनी के परिणय-सूत्र में आबद्ध हो सकता था अथवा सम्राट भी बन सकता था । लेकिन नहीं, उसका गरिमामय व्यक्तित्व तो ब्राह्मणत्व की इच्छाओं को समुद्र की तरह आत्मसात् कर लेता है । वर्षाकालीन उमड़ती हुई नदियों के जल को ग्रहण कर सागर जिस प्रकार निश्चित, स्थिर, शान्त और गंभीर बना रहता है, उसी प्रकार अनेक कामनाएँ ब्राह्मणत्व की महिमा से पूर्ण चाणक्य को अपने मार्ग से विचलित नहीं करती हैं। यही ब्राह्मण का आदर्श है।
भावपल्लवन के अभ्यास के लिए कुछ प्रसिद्ध वाक्य या अवतरण दिये जा रहे हैंः-
1. बुद्धिमान लोग गुरु का ऋण बहुत बड़ा मानते हैं, क्योंकि और ऋण तो आसानी से लौटाये जा सकते हैं-ज्ञानदान का ऋण सबके लिये लौटाना संभव नहीं है।
–महात्मा गांधी
2. जब तक माला गूंथी जाती है तब तक फूल मुरझा जाते हैं ।
3. आशा जीवन का लंगर है, उसका सहारा छोड़ने से मनुष्य भवसागर में डूब जाता है। बिना हाथ-पाँव फैलाए केवल आशा करने से काम नहीं चलता ।
हिंदी माध्यम नोट्स
Class 6
Hindi social science science maths English
Class 7
Hindi social science science maths English
Class 8
Hindi social science science maths English
Class 9
Hindi social science science Maths English
Class 10
Hindi Social science science Maths English
Class 11
Hindi sociology physics physical education maths english economics geography History
chemistry business studies biology accountancy political science
Class 12
Hindi physics physical education maths english economics
chemistry business studies biology accountancy Political science History sociology
English medium Notes
Class 6
Hindi social science science maths English
Class 7
Hindi social science science maths English
Class 8
Hindi social science science maths English
Class 9
Hindi social science science Maths English
Class 10
Hindi Social science science Maths English
Class 11
Hindi physics physical education maths entrepreneurship english economics
chemistry business studies biology accountancy
Class 12
Hindi physics physical education maths entrepreneurship english economics